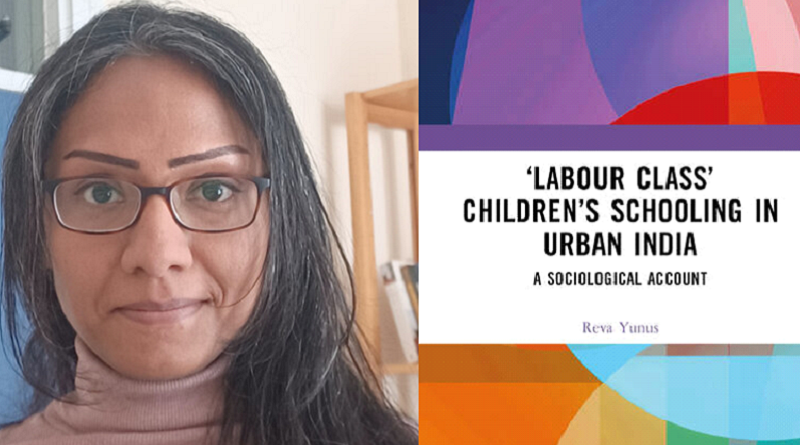समानांतर सिनेमा का आंदोलन और मलयालम सिनेमा का योगदान : Part-2

By मनीष आज़ाद
भारतीय फ़िल्मों और उस पर नक्सलबाड़ी आन्दोलन के असर की बात करें तो मलयालम फ़िल्मों पर उसका गहरा असर दिखता है। यहाँ एक बड़ा नाम ‘जॉन अब्राहम’ का है।
वे ‘ऋत्विक घटक’ के शिष्य थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि समानान्तर सिनेमा में जो लोग सक्रिय थे, वो आपस में भी एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए थे। ‘मणि कौल’ ऋत्विक घटक, के शिष्य थे।
जॉन अब्राहम ने मणि कौल की एक फ़िल्म ‘उसकी रोटी’ में सहायक डायरेक्टर की भूमिका निभाई थी।
गोविन्द निहलानी ने श्याम बेनेगल की फ़िल्मों में सहायक डायरेक्टर की भूमिका निभाई हैं। जॉन अब्राहम ने ‘पुणे फ़िल्म संस्थान’ से पढ़ाई की।
ये भी पढ़ें-
- थर्ड वर्ल्ड सिनेमा, समानांतर सिनेमा और सामाजिक आन्दोलन का प्रभाव- Part-1
- मट्टो की साइकिलः यह फिल्म हर मज़दूर को क्यों देखनी चाहिए?

चंदे से बनी फ़िल्म
जॉन अब्राहम ने 1986 में ‘अम्मा आर्यान’ (Amma Ariyan) बनायी थी जो नक्सलबाड़ी पृष्ठभूमि पर थी। बहुत बेहतरीन फ़िल्म है ये। लेकिन जॉन अब्राहम का इससे भी बड़ा योगदान था, ‘ओदेशा कलेक्टिव फ़िल्म सोसायटी’ बनाना।
नक्सलबाड़ी आन्दोलन के बाद से फ़िल्म सोसाइटी की बाढ़ सी आ गयी थी। हर जगह एक फ़िल्म सोसायटी बनती थी, उस फ़िल्म सोसाएटी के माध्यम से फ़िल्में दिखाई जाती थीं। उस पर गंभीरता से चर्चा होती थी। कई जगह तो उस फ़िल्म सोसाइटी के चंदे से फ़िल्में तक बनी हैं।
‘अम्मा आर्यान’ फ़िल्म ‘ओदेशा कलेक्टिव फ़िल्म सोसायटी’ के चंदे से ही बनी थी। आप इसको आज के ‘क्राउड फंडिंग’ से कंफ्यूज मत कीजियेगा, ‘क्राउड फंडिंग’ भी बढ़िया चीज़ है। लोग मदद करते हैं।
लेकिन क्राउड फंडिंग में डायरेक्टर के साथ या फ़िल्म बनाने वाली यूनिट के साथ उस तरह का ‘आर्गेनिक रिलेशन’ नहीं रहता।
‘अदुरगोपाल कृष्णन’ ने भी अन्य लोगों के साथ मिलकर ‘चित्रलेखा फ़िल्म सोसायटी’ बनायी थी। इस सोसायटी ने भी उनकी फ़िल्म को फ़ंड किया था।
यहाँ पर जो व्यक्ति फ़िल्म के लिए पैसा देता था उसका फ़िल्म यूनिट के साथ एक ‘आर्गेनिक रिलेशन’ रहता था। वो कई बार महत्वपूर्ण सुझाव भी देता था।

‘द हॉन्टेड माइंड ‘
इसी रूप में फ़िल्म मेकिंग एक तरह से सामूहिक प्रयास होता था। हालाँकि बंगाल में सत्यजीत रे ने अन्य साथियों के साथ मिलकर काफ़ी पहले ही फ़िल्म सोसाइटी बना ली थी।
इस सोसाइटी के माध्यम से ही कलकत्ता के बुद्धिजीवियों व फ़िल्म प्रेमियों को बहुत सी फ़िल्में जैसे चार्ली चैप्लिन की, जॉन फोर्ड की, जीन रेना…. जैसे विश्व के प्रसिद्ध निर्देशकों की फ़िल्में देखने को मिली। यानी एक निरंतरता भी है। लेकिन नक्सलबाड़ी के बाद इसमें एक गुणात्मक छलांग आ गया।
इसी ‘ओदेशा कलेक्टिव फ़िल्म सोसाइटी’ के एक और फ़िल्मकार थे – ‘सत्यम’। सत्यम का फ़िल्म से ज़्यादा डॉक्युमेंट्री में बड़ी भूमिका थी। उन्होंने नक्सलबाड़ी के शहीद ‘कामरेड वर्गीस’ पर बहुत महत्वपूर्ण डाकूमेंट्री बनायी थी। वर्गीस नक्सलबाड़ी आन्दोलन में केरल के पहले शहीद थे, जिनको 1976 में पुलिस ने गोली मार दी थी।
कामरेड वर्गीज को जिसने गोली मारी थी, उसे यह घटना ज़िन्दगी भर परेशान करती रही। अपने ऊपर के ऑफिसर के कहने पर उसने निहत्थे वर्गीज को गोली मारी थी।
अपने तमाम अंतरद्वन्द के बाद अंततः 94-95 के आसपास उसने स्वीकार किया कि वर्गीज को फ़र्जी मुठभेड़ में मारा गया था । और उसने ‘फ़ला’ आफिसर के कहने पर खुद वर्गीज को गोली मारी थी।
उसके इसी अन्तरद्वन्द पर एक फ़ीचर फ़िल्म भी है जो 2007 में आई थी। लेकिन सबसे पहले सत्यम ने अपनी डॉक्युमेंट्री में उसके अंतरद्वन्द को पकड़ा कि कैसे ऑफ़िसर के कहने पर उसने गोली मार तो दी, लेकिन उसके बाद वह व्यक्ति तिल तिल मरता रहा। इस फ़िल्म का नाम ‘द हॉन्टेड माइंड ‘ (The Haunted Mind) है।
ये भी पढ़ें-
- ‘द फ़ैक्ट्री’ फ़िल्म दिखाती है, श्रम क़ानूनों को कांग्रेस ने रद्दी बना दिया था, बीजेपी ने उसे बस जामा पहनाया है
- एक ज़रूरी फ़िल्म ‘चिल्ड्रेन ऑफ हैवेन’; मासूमियत की खुशबू के 25 साल

अदूरगोपाल कृष्णन का सिनेमा
उसके बाद जो दूसरा नाम है वो अदूरगोपाल कृष्णन का नाम है जिन्होंने ‘चित्रलेखा फ़िल्म सोसाइटी’ बनायी थी। चित्रलेखा फ़िल्म सोसाइटी की पहली फ़िल्म ‘स्वयंवरम’ (Swayamvaram) थी। इन फ़िल्मों को आप देखेंगे तो पाएंगे कि इन फ़िल्मों में आउटडोर शूटिंग है, फ़िल्म मेकिंग के तमाम तामझाम एकदम नहीं है, लगभग सभी ऐसे नए कलाकार हैं जिन्होंने शायद ही कभी अभिनय किया हो।
‘स्वयम्वरम’ में जो नायिका है उसने तो पहले अभिनय किया था, (वह वहां की स्थापित ऐक्टर थी) लेकिन जो नायक है उसने पहले कभी अभिनय नहीं किया था। इसलिए ऐसी फ़िल्मों में एक अलग तरह की ताज़गी मिलती है। इ
सी फ़िल्म में स्लम में जब पति पत्नी रहने के लिए जाते है तो उनके बगल में एक वेश्या रहती है, उसके बगल में मज़दूर है यानी आपको एक पूरा सन्दर्भ दिखता है। पूरा समाज दिखता है।
तथाकथित मुख्यधारा के सिनेमा में कैमरा हमेशा हीरो पर फोकस रहता है। इसलिए ‘Third (world) Cinema’ क्लोज-अप का बहुत कम इस्तेमाल करता था। यहाँ कैमरा ना सिर्फ मुख्य कलाकारों पर फोकस करता है बल्कि उनके आसपास की जो चीजें हैं, परिस्थितियां हैं उसको भी फ्रेम में रखता है।
इससे कलाकारों की सामाजिक पहचान का पता चलता है, वे कहाँ रहते हैं, क्या उनकी सस्कृति है, क्या उनका समाज है आदि। आप हॉलीवुड-बॉलीवुड की फ़िल्में देखेंगे तो उसमे पूरा फोकस अक्षय कुमार, सलमान ख़ान या जो भी हीरो है उसी पर रहता है।
उसकी पहचान क्या है, वो कहाँ से पैसा कमाता हैं, उनकी सांस्कृतिक जड़ें क्या हैं, इसके बारे में ना कोई जानकारी होती है, ना उसको देने की कोई ज़रूरत समझी जाती है। क्योंकि वहाँ फ़िल्म एक ‘प्रोडक्ट’ है। इसलिए बहुत सारे फ़िल्म समीक्षक इसे फ़िल्म मानते ही नहीं हैं। इस फ़िल्म इंडस्ट्री से तो ‘प्रोडक्ट’ ही निकलेगा। कला तो उससे निकलेगी नहीं।

फ़िल्म ‘कुमाटी’ का असर
तीसरा महत्वपूर्ण नाम ‘जी अरविन्दम’ का है। इन्होंने भी बहुत सारी फ़िल्में बनायी। 72 में उन्होंने ‘कंचन सीता’ बनायी थी। यह राम और सीता की परम्परागत कहानी पर आधारित फ़िल्म है। इसमें उन्होंने राम के रूप में एक आदिवासी को चुना।
एक आदिवासी को राम की भूमिका देने के कारण उनपर काफी हमले हुए। और कई जगह उनकी फ़िल्मों को रोक दिया गया। फिर उसके 2-3 साल बाद उनकी एक बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म आई ‘कुमाटी’। कुमाटी वहां एक लोक फार्म है। फ़िल्म में एक जादूगर आता है, बच्चों को इकठ्ठा करता है और बच्चे जो चाहते हैं उनको वो बना देता है।
बच्चे पक्षी बनकर, बकरी बनकर , सांप बनकर खूब मस्ती करते हैं। फिर जाते समय जादूगर उन सब को वापस बच्चा बना देता है। इसी प्रक्रिया में एक बच्चा कुत्ता बनकर कहीं छुप जाता है, और जादूगर, जिसे कुमाटी बोलते है, चला जाता है।
अब वह साल भर बाद आएगा। तो साल भर इसे कुत्ता ही रहना पड़ेगा। साल भर तक ये बच्चा कुत्ता बनकर घूमता है चारों तरफ़। उसको पहली बार गुलामी का अर्थ पता चलता है। जब एक साल बाद कुमाटी आता है तो उसे दुबारा बच्चा बनाता है।
उसके बाद बच्चा जो पहला काम करता है वह यह कि घर में जाकर अपने तोते को आज़ाद कर देता है। क्योंकि कुत्ता बनकर उसको पता चल गया था कि गुलामी क्या होती है। बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है।
नक्सली आन्दोलन का प्रभाव था कि चीज़ों पर सवाल खड़े करो, जो रूढ़ियाँ हैं, उसको तोड़ो। ‘तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब’, तो जो मठ और गढ़ है हमारे दिमाग के, जो सामाजिक-सांस्कृतिक अवरोध हैं, उसको तोड़ती है ये सारी फ़िल्में।
इन फ़िल्मों में सीधे-सीधे कहीं नक्सलवाद की बात नहीं है, पर इस आन्दोलन की जो ‘सेन्सीबिलिटी’ थी, जो विचारधारा थी वो इन फ़िल्मों को खुले-छिपे रूप में प्रभावित कर रही थी।
ये भी पढ़ें-
- स्वतंत्रता आंदोलन के भुला दिए गए 15 नायक जिनसे कांपती थी अंग्रेज़ी हुकूमत: ‘द लास्ट हीरोज़’ का विमोचन
- ‘कैंडल्स इन द विंड’ : खुदकुशी के साये में पंजाब की महिलाओं की ज़िंदगी

1970 के दशक की प्रमुख फ़िल्में
उसके बाद नाम आता है, ‘पी. ए. बाकर’ का। इन्होंने कम फ़िल्में बनायीं हैं। बाकर ने 1975 में एक महत्वपूर्ण फ़िल्म बनायी जो नक्सल आन्दोलन पर ही आधारित थी। फ़िल्म का नाम था-‘व्हेन द रिवर कबानी टर्न्ड रेड’(When the River Kabani Turned Red). ‘कबानी’ केरल की एक नदी का नाम है। फ़िल्म का नाम ही बहुत कुछ कह देता है।
अब यदि हम उसी दौर के कन्नड़ सिनेमा की बात करें तो गिरीश कनार्ड, गिरीश कसारवेली, वी। बी। कारंत जैसे दिग्गजों का नाम सामने आता है। गिरीश कसारवेली ने 1977 में अनंतमूर्ती की कहानी ‘घटश्राद्ध’ पर एक फ़िल्म बनायी थी। ये हिंदी में “दीक्षा” नाम से बनी है। इसमे नाना पाटेकर दलित है, एक ब्राह्मण का बच्चा है।
उसको नहीं पता कि क्या छूआछूत है, वो नाना पाटेकर को सहज ही छूने जाता है तो नाना पाटेकर भागता है कि ब्राह्मण का बच्चा मुझे कैसे छू सकता है। फिर भागते हुए नाना पाटेकर को भी थोड़ा मज़ा आने लगता है। बच्चे को भी मज़ा आने लगता है। फिर नाना पाटेकर बच्चे के छूने से बचते हुए बोलता है- ‘मुझे पानी छू सकता, मुझे सूरज की रोशनी छू सकती, मुझे हवा छू सकती, लेकिन ब्राह्मण का बच्चा नहीं छू सकता’। कमाल का संवाद है यह, बेचैन कर देने वाला।
‘वी बी कारंत’ और ‘गिरीश कर्नाड’ ने 1972 में ‘वंशवृक्ष’ फ़िल्म बनाई। इसमे एक विधवा महिला के संघर्षों की कहानी है , वह भी बहुत मशहूर हुई थी। उसको नेशनल अवार्ड भी मिले थे।
असम में ‘जानू बरुआ’ का नाम है। इसके अलावा ‘भवेंद्र नाथ सैकिया’ का नाम है। जानू बरुआ ने हिंदी में भी काफी फ़िल्में बनाई हैं, ‘मैंने गाँधी को नहीं मारा’…आदि। असम में समानान्तर सिनेमा उतना मजबूत नहीं था। असम में फ़िल्म इंडस्ट्री भी काफी कमज़ोर है।
जानू बरुआ ने 83 में ‘अपरूपा’ बनाई थी। उसमें भूपेन हजारिका ने संगीत दिया था। ‘सुहासिनी मुले’ जो भुवन शोम की नायिका थी, उन्होंने यह फ़िल्म की थी। आज की शब्दावली में इसे एक ‘फ़िमिनिस्ट फ़िल्म’ भी कह सकते हैं।
ये भी पढ़ें-
- एक ज़रूरी फ़िल्म Mephisto: एक कलाकार जिसने अपनी आत्मा नाज़ियों को बेच दी
- घोड़े को जलेबी खिलाती और दर्शकों को Reality Trip कराती फ़िल्म

मणिपुरी फ़िल्म ‘My Son, My Precious’
इसी समय (1981) मणिपुर में भी एक अच्छी फ़िल्म बनी थी, ‘My Son, My Precious’, जहाँ पर एक टीचर एक अनाथ बच्चे को पढ़ाते हुए, उसके साथ इस कदर एक रिश्ते में बंध जाती है कि उस बच्चे के पिता का पता लगाने और उसको न्याय दिलाने के संघर्ष में शामिल हो जाती है। बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है। मणिपुर की फ़िल्म इंडस्ट्री भी काफ़ी कमजोर है। ज़्यादा फ़िल्में नहीं बनी है।
अब हम लोग आते हैं मराठी सिनेमा पर। मराठी सिनेमा काफी समृद्ध है। उसमें एक बड़ा नाम है- ‘जब्बार पटेल’ का। जब्बार पटेल ने वहां के ग्रामीण इलाके का जो वर्ग संघर्ष था, (वह सीधे–सीधे नक्सलबाड़ी से प्रभावित था) उस पर ‘सामना’ फ़िल्म बनाई।
उसमें कहीं भी नक्सल शब्द नहीं है, लेकिन उसमें जो वर्ग संघर्ष आ रहा है, वह इसी आन्दोलन की प्रेरणा से ही आ रहा है। यहाँ यह जानना भी ज़रूरी है कि मराठी नाटकों में उस वक़्त विजय तेंदुलकर का दबदबा था, उन्होंने नई धारा ही शुरू कर दी थी।
इस दौरान कई महत्वपूर्ण फ़िल्मों की स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखी। हिंदी की भी और मराठी की भी। ‘सामना’ के बाद ज़ब्बार पटेल की दूसरी फ़िल्म 1979 में राजनीतिक भ्रष्टाचार पर आई। नाम था- ‘सिंघासन’।
इसकी स्क्रिप्ट विजय तेंदुलकर ने ही लिखी थी। फिर आई ‘तीसरी आज़ादी’, जो दलित नज़रिए से रामायण, महाभारत को पुनर्व्याख्यायित करती है।
हमें यह भी याद रखना चाहिए कि विजय तेंदुलकर और महेश एन्चुक्वार ने कई उन हिंदी फ़िल्मों की भी स्क्रिप्ट लिखी जो सीधे-सीधे नक्सलवाद की विचारधारा या उसकी ‘सेंसिबिलिटी’ से प्रभावित थी।
लेख आगे भी जारी…
(लेखक प्रगतिशील फ़िल्मों पर लिखते रहे हैं। विश्व सिनेमा, समानांतर सिनेमा और सामाजिक आंदोलन के अंतरसंबंध को मोटा मोटी समझने के लिए लिखा गया ये एक लंबा लेख है जिसे पांच हिस्सो में बांटा गया है और शृंखला में प्रकाशित होगा। इस लेख की यह दूसरी कड़ी है। )
वर्कर्स यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए सब्स्क्रिप्शन ज़रूर लें- यहां क्लिक करें
(वर्कर्स यूनिटी के फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें। मोबाइल पर सीधे और आसानी से पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें।)